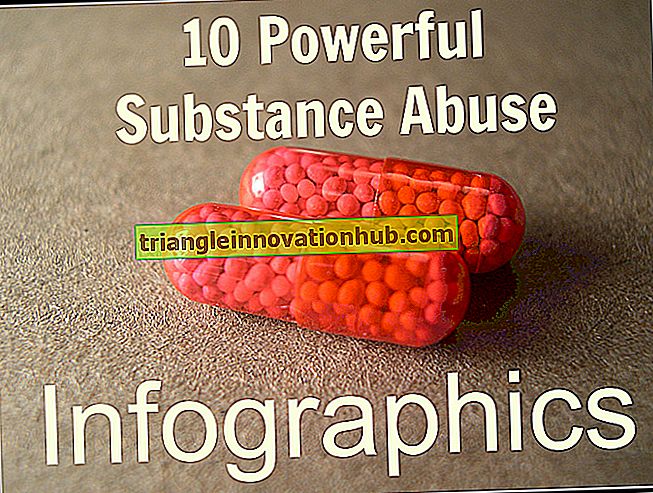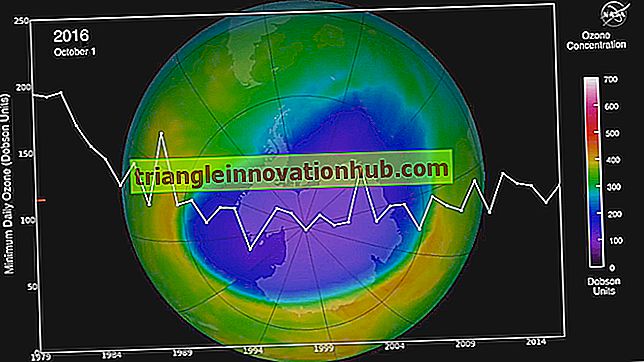स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती
स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती का जन्म 1824 में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता शिव के उपासक थे। दयानंद ने अपने पिता की सलाह पर वेदों को हृदय से लगा लिया। धीरे-धीरे उसके मन में एक बदलाव आया। जब उन्होंने मूर्तियों के बारे में सोचा, तो उनके मन में संदेह पैदा हुआ कि क्या उस रूप में भगवान के बारे में सोचना सही था।
अपनी युवावस्था में जब वह शिवरात्रि की रात में पूजा करने के लिए शिव की छवि के सामने खड़े हो गए तो एक प्रश्न अपने आप में उठ गया “क्या यह संभव है कि यह मूर्ति जो सभी खातों के अनुसार चलती है, खाती है, सोती है, पीती है, अपने त्रिशूल धारण करती है हाथ, ढोल पीटता है और पुरुषों पर श्राप का उच्चारण कर सकता है, वह महान देवता हो सकता है, महादेव सर्वोच्च देवता हैं। ”वह विश्वास नहीं कर सकता था कि मूर्ति भगवान थी। इन उत्तरों की खोज में, वह 21 साल की उम्र में एक सन्यासी बन गया और यहाँ और वहाँ आश्चर्य किया कि भगवान के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए।
अंत में उन्हें विश्वास हो गया कि वेदों में सर्वोच्च सत्य निहित है। वेदों में, भगवान को एक निराकार, सर्वशक्तिमान निर्माता के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने प्रकृति में खुद को प्रकट किया। प्राचीन काल में आर्यों को वेदों से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ने उन्हें वास्तविकता के निकट लाया। वैदिक समाज पुरुषों की इक्विटी पर आधारित एक आदर्श समाज था और कोई भी जाति व्यवस्था नहीं थी, भले ही समाज को उनके पेशे जैसे पूजा, युद्ध, कृषि और व्यापार और सामाजिक सेवा के अनुसार चार प्राकृतिक वर्गों में विभाजित किया गया था।
वैदिक समय के दौरान कोई अस्पृश्यता नहीं थी और महिलाएं समाज में सम्मान और स्वतंत्रता का आनंद ले रही थीं। दयानंद महसूस कर सकते थे कि बाद के हिंदू धर्म गलत हो गए और जीवन के मूल्यों को खो दिया। इसने कई गलत मान्यताओं को समायोजित किया जिसने सामाजिक एकता की रस्सी को तोड़ने वाले पुरुषों के बीच विभाजन पैदा किया। दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय भावना को जगाने के उद्देश्य से 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज शिक्षा का प्रसार करने और विशेष रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश में वैदिक धर्म और भारतीय समाज को सबसे स्वाभाविक के रूप में सामाजिक सुधार लाने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली संगठन बन गया और दयानंद भारत के खोए हुए आदर्शों को पुनर्जीवित करना चाहते थे।
इस प्रकार उन्होंने नारा दिया "बैक टू वेद"। इसका उद्देश्य भारतीयों को ईश्वर और वेदों में पूर्ण विश्वास के बारे में सिखाना था। उन्होंने वेदों को सच्चे ज्ञान का धर्मग्रंथ बताया और कहा कि "आर्यों का पहला कर्तव्य है कि वेदों को ध्यान से पढ़ें और उन्हें समझें।" आर्य समाज ने ब्राह्मणों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया और छवि पूजा की प्रथा को नकार दिया। दयानंद ने अंधविश्वास की निंदा की। आर्य समाज ने वैदिक समाज में काम के अनुसार चार जातियों के लिए प्रार्थना की। इसने अनगिनत उपजातियों की अवधारणा की आलोचना की जिसने भारतीय एकता को नष्ट कर दिया था। दयानंद ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत की। उन्होंने अछूतों को जाति के हिंदुओं की श्रेणी में लाने की कोशिश की।
शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने सराहनीय कार्य किया। इसने 1902 में वैदिक आदर्शों के अनुसार गुरुकुलों या शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। गुरुकुल आश्रमों में, विद्यार्थियों के शरीर, मन और चरित्र के विकास पर जोर दिया गया था। विज्ञान और हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान और कला के विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता था।
1883 में दयानंद की मृत्यु हो गई लेकिन आर्य समाज ने पूरे जोश के साथ काम करना जारी रखा। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को तर्कसंगत बनाया और हिंदुओं के बीच गर्व की भावना लाई। समाज को नए दृष्टिकोण के साथ उदारीकृत करके समाज ने सामाजिक एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एकता हुई। जाति, पंथ, समुदाय, एक लिंग के बावजूद सभी की समानता के विचार के माध्यम से, समाज ने बहुत जल्दी भारतीयों में लोकतांत्रिक चेतना की भावना विकसित की। 1905-10 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ब्रिटिश सरकार ने आर्य समाज पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने का आरोप लगाया और ब्रिटिश संप्रभुता के लिए एक खतरे के रूप में देखा।